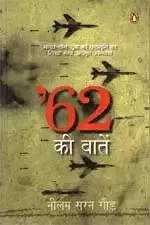|
विविध उपन्यास >> 62 की बातें 62 की बातेंनीलम सरन गौड़
|
263 पाठक हैं |
||||||
भारत-चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया अद्भुत उपन्यास...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
’62 की बातें 1995 में प्रकाशित नीलम सरन गौड़ के
अंग्रेज़ी उपन्यास स्पीकिंग ऑफ़’62 का हिंदी अनुवाद है, जो लेखिका
ने स्वयं किया है। इस मनोरंजक उपन्यास में 1962 के भारत-चीन युद्ध को छह
नटखट बच्चों की नज़र से देखा गया है। छह बच्चे जो युद्ध का मतलब समझने के
लिए जूझ रहे हैं और अपने आसपास उससे होने वाले असर को देख रहे हैं।
इतिहास, ख़ानदानी कहानियां, समकालीन राजनैतिक विवाद, बचपन की शैतान हरकतों
को हास्य रस की ताज़गी के साथ बयां किया गया है। कुछ ऐसे मुद्दों की भी
चर्चा की गई है जो आज भी मौजूद हैं, शायद और भी गंभीर रूप में।
‘ढेर सारी मौज-मस्ती और ढेर सारे चिंतन योग्य आकस्मिक विचार... नीलम सरन गौड़ बड़ी सफ़ाई से अहंकार और नक़ली आडंबर के बुलबुलों को कोंच सकती हैं। हमारे देश को ऐसे कथाकारों की ज़रूरत है, जो विविधताओं का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं।’’
‘ढेर सारी मौज-मस्ती और ढेर सारे चिंतन योग्य आकस्मिक विचार... नीलम सरन गौड़ बड़ी सफ़ाई से अहंकार और नक़ली आडंबर के बुलबुलों को कोंच सकती हैं। हमारे देश को ऐसे कथाकारों की ज़रूरत है, जो विविधताओं का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं।’’
–प्रेमा नंदकुमार, डेकन हेरल्ड
इस (उपन्यास) की प्रत्येक कहानी एक अलग समाज
को दर्शाती
है, पूर्णरूप से तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक जो न सिर्फ़ सुपठनीय है,
बल्कि कलात्मक ढंग से गुथी हुई भी है।’
–इंडियन रीव्यू ऑफ़ बुक्स
Speaking of ’62, Neelum Saran Gour
आवरण डिज़ाइन : पूजा आहूजा
आवरण डिज़ाइन : पूजा आहूजा
सफ़ेद पत्थरों का रेगिस्तान
वह छोटी सी किताब एक छोटी सी जंग के बारे में
है। इतनी
छोटी कि वह अतीत के एक पैराग्राफ़ में समा सकती है और शायद दो लाइनों में
भी। लेकिन हम लोगों के लिए वह एक संवेदनापूर्ण यादगार बन गई है और हम उसे
मन में दोहराते हैं इतिहास पढ़ने वालों की तरह नहीं, जो घटना, वजह और अर्थ
जोड़ते जाते हैं, बल्कि केवल याददाश्त की तिलिस्मी और असमान पंक्तियों
में।
तीस साल गुज़र गए हैं। उस सड़क का दोबारा नामकरण हो गया है। वह मकान अब नहीं है। लेकिन जहां तक हम लोगों की बात है 1962 के हिंदुस्तान-चीन युद्ध की भूमि उस रसोईघर का टूटा-फूटा फ़र्श था। मैकमोहन रेखा मसालों के नियामतख़ाने से लेकर पत्थर की सिल तक खिंची थी और अरब-सागर चावल और आटे की हांडियों के पीछे था। मैं आपको उस रसोईघर के बारे में बताऊं। ज़मीन टूट-फूट चुकी थी, ईश्वर जाने कैसे, उसका सीमेंट पैरों तले चूर-चूर, और अंदर की ईंटें मुंह फाड़े, दांत निकाले, तह पर तह पहाड़ियों की सिलवटों की तरह हो गई थीं। पिताजी स्कूल मास्टर थे। उम्दा स्कूल मास्टर, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मुहल्ले वाले उन्हें ‘मास्टर-साहब’ बुलाते थे। काश कि मैं सादगी का एक नया डेकोर निकालता–पचास के दशक के स्कूल मास्टर का कमरा। नंगी फ़र्श, किताबों के रैक, दीवार पर कपड़ों की खूंटी जिस पर टंगे रहते कोट, छाता, छड़ी और एक सोला टोपी। दुबली सी मेज़, दो सीधी पीठ वाली कुर्सियां, चश्मे, तख़्त। सींकचों वाली खिड़की, बेरंग से पर्दे से आधी ढकी। दीवार पर रामकृष्ण परमहंस की तस्वीर। यही उनके बैठने और पढ़ने का कमरा था। कमरे के मिज़ाज में एक अजीब रईसी थी, सुलझे मूल्यों का सलीक़ा, हर चीज़ आवश्यकता के हिसाब से चुनी हुई। लेकिन रसोईघर उनका दरबार था और हम थे उनकी प्रजा। हम छह थे। रसोईघर हमारे पढ़ाई की जगह थी। ऊबड़-खाबड़ ज़मीन हमारे इतिहास और भूगोल के पाठ के लिए आदर्श मॉडल थी। विदेशी हमलावर उधर बाईं तरफ़ से देश में दाख़िल होते और बीच के समतल हिस्से में फैल जाते। यही जगह थी जहां हम आर्य-द्रविड़ और मुग़ल-राजपूत बनकर खेला करते थे।
पिताजी दिलचस्प अध्यापक थे। मुझे याद है घंटों तक खड़े होकर सितारों का नक्शा पढ़ना। मैं तो ख़ुद भी ओरायन नक्षत्र बनकर, बेल्ट पहने, कुत्ता लेकर दौड़ता था। और वह ध्रुवतारे की तलाश। वहीं तो था, अकेला, कुछ खोया सा, थोड़ा असंभव सा, और देखते-देखते, एकटकी नज़र गाड़े, ऐसा लगता कि वह नील-श्यामल आकाश बाढ़ की तरह अपनी विराट लपेट में हमें डुबो देता। ऐसा लगता कि मस्तिष्क में सितारों के झुंड उफ़नते, छलकते, अपनी भयानक भंवर में हमें क़ैद कर लेते। फिर भी हम ताकते रहते, विस्मित आकर्षण में। लंबी सांस लेते, निश्चित कि कुछ सितारे शायद सूखे गले में खिंच आएं। बालों और चेहरे पर जैसे झीनी रुपहली धूल आ पड़ी होती। फिर गर्दन पर सिरहन उठती और मैं नहा जाता चंद्रमा की श्वेत शीत-लहर में। यही अनुभव था गर्मियों की रातों में आकाश को निहारने का। और अंत तक ध्रुवतारा दूर प्रतीक्षा करता, मुंह फेरे; और मेरी नज़र उस तक, आकाश के उस पार, न पहुंच पाती। रूसियों ने एक स्पुटनिक भेजा था। गर्मियों की रातों में हम उसके निकलने का इंतज़ार करते।
कभी-कभी इतिहास पलट जाता है। राजपूत मुग़ल को पटक देता और आर्य पिनपिनाता हुआ मां के पास शिकायत करता पहुंचता कि द्रविड़ ने उसकी नाक पर घूंसा मार दिया है। और 1962 तो एक ख़ास वर्ष था। उस साल हम हिंदी-चीन बन गए।
चीन तो एक रोमांच-भरा स्थान था। चीन था कुबला ख़ां और मारको पोलो, रेशम और चाय, बारूद और विशाल, पटाख़े और पतंग। नूडल्स से हम नावाक़िफ़ थे। पिताजी लिन यूटांग का भी अक्सर ज़िक्र करते। सब कुछ उस चमत्कारी रसोईघर में। काश कि मैं उस जगह को ठीक बयां कर पाता क्योंकि हमारा घर एक रसोई-प्रधान घर था।
एक बड़ा सा खपरैल वाला कमरा, एक तरफ से विभाजित, पवित्र और हमारे लिए वर्जित, जलते चूल्हे का गर्भ गृह। यहां मिट्टी के लेप वाले फ़र्श पर बैठकर मां खाना पकाती थीं। आग की नीली-सुनहली पंखुड़ियां खौलती कढ़ाही को साधे रखतीं और धुएं की काली श्वास पीछे की दीवार पर अपनी स्याह का केंचुल त्यागती। यहां मां खाना परोसतीं और मानव जाति पर निर्णायक भाषण देतीं। रसोईघर के दूसरे, कम गंभीर हिस्से में हमारी टूटी सिकुड़ी ज़मीन थी, चिटकी, गढ्डीली, दंतीली।
यहां हम बैठते थे। लकड़ी के पीढ़ों पर, अर्ध-गोलाई में। सिर पर टिमटिमाता एक पुराना बल्ब—एक कामचलाऊ कनेक्शन जो छप्पर के नीचे पुरानी बल्ली से लटका था। छप्पर के जर्जर ताने-बाने से टपकते सूरज के धूल-धूसरित मोती और बरसात में बारिश की भटकी छींटें। शाम की परछाइयों की परत भिन्न-भिन्न प्रकार से घुली होतीं। हालांकि बल्ब की रोशनी बहुत हल्की थी, फिर भी वह पूरी तरह से एक विश्वसनीय और ज़िम्मेदार बल्ब था। आजकल के इन मनचले लैम्पों की तरह नहीं जो जब देखो हमें अंधकार में डुबो देते हैं। 1962 घटित हुआ वहीं रसोईघर में। दूध-भात खाते-खाते हमको समझाया गया काराकोरम पहाड़ का लोचपूर्ण आकार और मानचित्र में नेफ़ा (NEFA) की छाया।
वह भी उन अनंत, शांत ग्रीष्मकालों में से एक था। हर शाम हम आंगन में छिड़काव करते और सूखी पृथ्वी पर फुहार की आदि सुगंध की याद आज भी मन में कसक जीवित कर देती है। कटहल के पेड़ और पुराने पीपल के तले दर्जन भर सफ़ेद चादरों वाली चारपाइयों की क़तार बिछ जाती। सफ़ेद मच्छरदानियां कस दी जातीं बासों पर। खड़खड़ाता टेबल फ़ैन भीनी हवा को फड़का देता।
और हम ख़रबूज़े और मोटे-मोटे आम काटते। रात की रानी की ख़ुशबू मिश्रित होती पुदीने, इमलियों और कच्चे आमों की खटास में। क्या विचित्र नाम थे उन आमों के—लाल दीया, दिल-पसंद, ख़ुदा-बहिश्त, तोता-पारी ! हम आम के छिलकों के लंबे फ़ीतों से मालाएं बनाते और अपने कुत्तों, शैतान और कालू का माल्यारोपण करते।
बाग़ीचे के अंदर, नीबू के पेड़ों के नीचे, तुलसी के सामने, मां संध्या-दीपक जलातीं। क्या विस्मय और सन्नाटा, बाग़ीचे में इकलौते दीपक के अर्धप्रकाश में ! और इतने पतंगों और कीड़े-मकोड़ों का आक्रमण होता, जो उस रोशनी की लौ में गिरफ़्तार हो जाते और पेड़ों की डालों और झाड़ियों की चुन्नटों में छिपे होते अदृश्य, भिनभिनाते झींगुर, जो रात की तह में सुराख़ करते धैर्यपूर्वक सुराख करते जाते, जब तक सुबह तक सुरंग न बन जाती।
मैं नहीं उम्मीद करता कि उस तरह गर्मियों की रातों में, सितारों के तले, हम फिर कभी सो सकेंगे। सब लोग कहते हैं कि यह सब ख़तरनाक हो गया है। लेकिन मुझे याद है कि किस तरह झाड़ियों में जुगनू जल उठते थे और नींद हवा में घुल सी जाती थी। दिमाग़ में कोई भी भगदड़ न थी। सूर्योदय के साथ आंखें ख़ुद-ब-ख़ुद खुल जातीं प्रकृति की किसी प्राचीन लय के अनूकूल, और फिर कुछ देर तक हम पड़े रहते उन सफ़ेद लम्हों में, उन सूक्ष्म, स्फ़टिक आहटों को आज़माते। आज भी, तीस सालों के बाद, मैं उन आहटों को गिन सकता हूं उसी पुराने क्रम में।
पहले बाग़ीचे का नल चहकता—हमारी नींद के स्वर से थोड़ा ऊंचा और नीबू के पेड़ की कोयलों से थोड़ा नीचा। फिल नल का पानी, पंख फैलाता, बिखर जाता काई से ढके पुराने पत्थर की सिल्ली पर, शीतल, मीठे, रुकते-हांफते झोंकों में। फिर हथौड़े की आवाज़ आती, कोयले को ईंट पर तोड़ते हुए और ताड़-पत्ते के पंखे की सरसराहट। कुछ देर में चूल्हे से धुआं उठता। चूल्हे का पेट कंडियों से भरा होता और उसका बड़ा सा मुंह सुलगती लकड़ियों से ठुंसा रहता। फिर मंजते बर्तनों की आवाज़ आती, पीतल का घंटा तांबे की कटोरी पर गूंजता—नारियल की जटा और राख की रगड़ पर भुनभुनाते बर्तन, नल और थालियों का जोशीला झाला बजाते बर्तन, बातचीत करते, झंकारते, नहाते बर्तन। ये सब थे रसोईघर के स्वर।
तीस साल गुज़र गए हैं। उस सड़क का दोबारा नामकरण हो गया है। वह मकान अब नहीं है। लेकिन जहां तक हम लोगों की बात है 1962 के हिंदुस्तान-चीन युद्ध की भूमि उस रसोईघर का टूटा-फूटा फ़र्श था। मैकमोहन रेखा मसालों के नियामतख़ाने से लेकर पत्थर की सिल तक खिंची थी और अरब-सागर चावल और आटे की हांडियों के पीछे था। मैं आपको उस रसोईघर के बारे में बताऊं। ज़मीन टूट-फूट चुकी थी, ईश्वर जाने कैसे, उसका सीमेंट पैरों तले चूर-चूर, और अंदर की ईंटें मुंह फाड़े, दांत निकाले, तह पर तह पहाड़ियों की सिलवटों की तरह हो गई थीं। पिताजी स्कूल मास्टर थे। उम्दा स्कूल मास्टर, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मुहल्ले वाले उन्हें ‘मास्टर-साहब’ बुलाते थे। काश कि मैं सादगी का एक नया डेकोर निकालता–पचास के दशक के स्कूल मास्टर का कमरा। नंगी फ़र्श, किताबों के रैक, दीवार पर कपड़ों की खूंटी जिस पर टंगे रहते कोट, छाता, छड़ी और एक सोला टोपी। दुबली सी मेज़, दो सीधी पीठ वाली कुर्सियां, चश्मे, तख़्त। सींकचों वाली खिड़की, बेरंग से पर्दे से आधी ढकी। दीवार पर रामकृष्ण परमहंस की तस्वीर। यही उनके बैठने और पढ़ने का कमरा था। कमरे के मिज़ाज में एक अजीब रईसी थी, सुलझे मूल्यों का सलीक़ा, हर चीज़ आवश्यकता के हिसाब से चुनी हुई। लेकिन रसोईघर उनका दरबार था और हम थे उनकी प्रजा। हम छह थे। रसोईघर हमारे पढ़ाई की जगह थी। ऊबड़-खाबड़ ज़मीन हमारे इतिहास और भूगोल के पाठ के लिए आदर्श मॉडल थी। विदेशी हमलावर उधर बाईं तरफ़ से देश में दाख़िल होते और बीच के समतल हिस्से में फैल जाते। यही जगह थी जहां हम आर्य-द्रविड़ और मुग़ल-राजपूत बनकर खेला करते थे।
पिताजी दिलचस्प अध्यापक थे। मुझे याद है घंटों तक खड़े होकर सितारों का नक्शा पढ़ना। मैं तो ख़ुद भी ओरायन नक्षत्र बनकर, बेल्ट पहने, कुत्ता लेकर दौड़ता था। और वह ध्रुवतारे की तलाश। वहीं तो था, अकेला, कुछ खोया सा, थोड़ा असंभव सा, और देखते-देखते, एकटकी नज़र गाड़े, ऐसा लगता कि वह नील-श्यामल आकाश बाढ़ की तरह अपनी विराट लपेट में हमें डुबो देता। ऐसा लगता कि मस्तिष्क में सितारों के झुंड उफ़नते, छलकते, अपनी भयानक भंवर में हमें क़ैद कर लेते। फिर भी हम ताकते रहते, विस्मित आकर्षण में। लंबी सांस लेते, निश्चित कि कुछ सितारे शायद सूखे गले में खिंच आएं। बालों और चेहरे पर जैसे झीनी रुपहली धूल आ पड़ी होती। फिर गर्दन पर सिरहन उठती और मैं नहा जाता चंद्रमा की श्वेत शीत-लहर में। यही अनुभव था गर्मियों की रातों में आकाश को निहारने का। और अंत तक ध्रुवतारा दूर प्रतीक्षा करता, मुंह फेरे; और मेरी नज़र उस तक, आकाश के उस पार, न पहुंच पाती। रूसियों ने एक स्पुटनिक भेजा था। गर्मियों की रातों में हम उसके निकलने का इंतज़ार करते।
कभी-कभी इतिहास पलट जाता है। राजपूत मुग़ल को पटक देता और आर्य पिनपिनाता हुआ मां के पास शिकायत करता पहुंचता कि द्रविड़ ने उसकी नाक पर घूंसा मार दिया है। और 1962 तो एक ख़ास वर्ष था। उस साल हम हिंदी-चीन बन गए।
चीन तो एक रोमांच-भरा स्थान था। चीन था कुबला ख़ां और मारको पोलो, रेशम और चाय, बारूद और विशाल, पटाख़े और पतंग। नूडल्स से हम नावाक़िफ़ थे। पिताजी लिन यूटांग का भी अक्सर ज़िक्र करते। सब कुछ उस चमत्कारी रसोईघर में। काश कि मैं उस जगह को ठीक बयां कर पाता क्योंकि हमारा घर एक रसोई-प्रधान घर था।
एक बड़ा सा खपरैल वाला कमरा, एक तरफ से विभाजित, पवित्र और हमारे लिए वर्जित, जलते चूल्हे का गर्भ गृह। यहां मिट्टी के लेप वाले फ़र्श पर बैठकर मां खाना पकाती थीं। आग की नीली-सुनहली पंखुड़ियां खौलती कढ़ाही को साधे रखतीं और धुएं की काली श्वास पीछे की दीवार पर अपनी स्याह का केंचुल त्यागती। यहां मां खाना परोसतीं और मानव जाति पर निर्णायक भाषण देतीं। रसोईघर के दूसरे, कम गंभीर हिस्से में हमारी टूटी सिकुड़ी ज़मीन थी, चिटकी, गढ्डीली, दंतीली।
यहां हम बैठते थे। लकड़ी के पीढ़ों पर, अर्ध-गोलाई में। सिर पर टिमटिमाता एक पुराना बल्ब—एक कामचलाऊ कनेक्शन जो छप्पर के नीचे पुरानी बल्ली से लटका था। छप्पर के जर्जर ताने-बाने से टपकते सूरज के धूल-धूसरित मोती और बरसात में बारिश की भटकी छींटें। शाम की परछाइयों की परत भिन्न-भिन्न प्रकार से घुली होतीं। हालांकि बल्ब की रोशनी बहुत हल्की थी, फिर भी वह पूरी तरह से एक विश्वसनीय और ज़िम्मेदार बल्ब था। आजकल के इन मनचले लैम्पों की तरह नहीं जो जब देखो हमें अंधकार में डुबो देते हैं। 1962 घटित हुआ वहीं रसोईघर में। दूध-भात खाते-खाते हमको समझाया गया काराकोरम पहाड़ का लोचपूर्ण आकार और मानचित्र में नेफ़ा (NEFA) की छाया।
वह भी उन अनंत, शांत ग्रीष्मकालों में से एक था। हर शाम हम आंगन में छिड़काव करते और सूखी पृथ्वी पर फुहार की आदि सुगंध की याद आज भी मन में कसक जीवित कर देती है। कटहल के पेड़ और पुराने पीपल के तले दर्जन भर सफ़ेद चादरों वाली चारपाइयों की क़तार बिछ जाती। सफ़ेद मच्छरदानियां कस दी जातीं बासों पर। खड़खड़ाता टेबल फ़ैन भीनी हवा को फड़का देता।
और हम ख़रबूज़े और मोटे-मोटे आम काटते। रात की रानी की ख़ुशबू मिश्रित होती पुदीने, इमलियों और कच्चे आमों की खटास में। क्या विचित्र नाम थे उन आमों के—लाल दीया, दिल-पसंद, ख़ुदा-बहिश्त, तोता-पारी ! हम आम के छिलकों के लंबे फ़ीतों से मालाएं बनाते और अपने कुत्तों, शैतान और कालू का माल्यारोपण करते।
बाग़ीचे के अंदर, नीबू के पेड़ों के नीचे, तुलसी के सामने, मां संध्या-दीपक जलातीं। क्या विस्मय और सन्नाटा, बाग़ीचे में इकलौते दीपक के अर्धप्रकाश में ! और इतने पतंगों और कीड़े-मकोड़ों का आक्रमण होता, जो उस रोशनी की लौ में गिरफ़्तार हो जाते और पेड़ों की डालों और झाड़ियों की चुन्नटों में छिपे होते अदृश्य, भिनभिनाते झींगुर, जो रात की तह में सुराख़ करते धैर्यपूर्वक सुराख करते जाते, जब तक सुबह तक सुरंग न बन जाती।
मैं नहीं उम्मीद करता कि उस तरह गर्मियों की रातों में, सितारों के तले, हम फिर कभी सो सकेंगे। सब लोग कहते हैं कि यह सब ख़तरनाक हो गया है। लेकिन मुझे याद है कि किस तरह झाड़ियों में जुगनू जल उठते थे और नींद हवा में घुल सी जाती थी। दिमाग़ में कोई भी भगदड़ न थी। सूर्योदय के साथ आंखें ख़ुद-ब-ख़ुद खुल जातीं प्रकृति की किसी प्राचीन लय के अनूकूल, और फिर कुछ देर तक हम पड़े रहते उन सफ़ेद लम्हों में, उन सूक्ष्म, स्फ़टिक आहटों को आज़माते। आज भी, तीस सालों के बाद, मैं उन आहटों को गिन सकता हूं उसी पुराने क्रम में।
पहले बाग़ीचे का नल चहकता—हमारी नींद के स्वर से थोड़ा ऊंचा और नीबू के पेड़ की कोयलों से थोड़ा नीचा। फिल नल का पानी, पंख फैलाता, बिखर जाता काई से ढके पुराने पत्थर की सिल्ली पर, शीतल, मीठे, रुकते-हांफते झोंकों में। फिर हथौड़े की आवाज़ आती, कोयले को ईंट पर तोड़ते हुए और ताड़-पत्ते के पंखे की सरसराहट। कुछ देर में चूल्हे से धुआं उठता। चूल्हे का पेट कंडियों से भरा होता और उसका बड़ा सा मुंह सुलगती लकड़ियों से ठुंसा रहता। फिर मंजते बर्तनों की आवाज़ आती, पीतल का घंटा तांबे की कटोरी पर गूंजता—नारियल की जटा और राख की रगड़ पर भुनभुनाते बर्तन, नल और थालियों का जोशीला झाला बजाते बर्तन, बातचीत करते, झंकारते, नहाते बर्तन। ये सब थे रसोईघर के स्वर।
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book